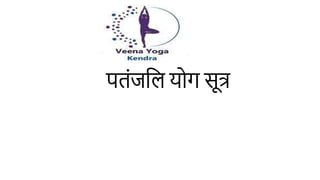
Yoga Philosophy.pptx
- 2. महर्षि पतञ्जर्ि की प्रार्िना • योगेन र्ित्तस्य पदेन वािाां, मिां शरीरस्य ि वैद्यक े न। • योऽपाकरोत् तां प्रवरां मुनीनाां, पतांजर्िप्राांजर्िरानतोऽस्मि।। अर्ि: • श्लोक का अर्िप्राय है र्क 'योगशास्त्र से मन का, व्याकरण शास्त्र से वाणी वाणी का और वैद्यक शास्त्र से तन का मि नष्ट करने वािे पतांजर्ि मुर्न क े सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ।'
- 3. • पातंजि योगसूत्र, योग दर्शन का मूि ग्रंथ है। यह षड दर्शनों में से एक र्ास्त्र है और योगर्ास्त्र का एक ग्रंथ है। योगसूत्रों की रचना ३००० साि क े पहिे पतंजलि ने की। इसक े लिए पहिे से इस लिषय में लिद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग लकया। • योगसूत्र में लचत्त को एकाग्र करक े ईश्वर में िीन करने का लिधान है। पतंजलि क े अनुसार लचत्त की िृलत्तयों को चंचि होने से रोकना (लचत्तिृलत्तलनरोधः) ही योग है। अथाशत् मन को इधर-उधर भटकने न देना, क े िि एक ही िस्तु में स्थथर रखना ही योग है।
- 4. • पतंजलि का योगदर्शन, समालध, साधन, लिभूलत और क ै िल्य इन चार पादों या भागों में लिभक्त है। • समार्िपाद में यह बतिाया गया है लक योग क े उद्देश्य और िक्षण क्या हैं और उसका साधन लकस प्रकार होता है। • सािनपाद में क्लेर्, कमशलिपाक और कमशफि आलद का लििेचन है। • र्विूर्तपाद में यह बतिाया गया है लक योग क े अंग क्या हैं, उसका पररणाम क्या होता है और उसक े द्वारा अलणमा, मलहमा आलद लसस्ियों की लकस प्रकार प्रास्ि होती है। • क ै वल्यपाद में क ै िल्य या मोक्ष का लििेचन लकया गया है
- 5. • संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है लक मनुष्य को अर्वद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अलभलनिेर् ये पााँच प्रकार क े क्लेर् होते हैं, और उसे कमश क े फिों क े अनुसार जन्म िेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि ने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राि करने का उपाय योग बतिाया है और कहा है लक क्रमर्ः योग क े अंगों का साधन करते हुए मनुष्य लसि हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राि कर िेता है।
- 6. • ईश्वर क े संबंध में पतंजलि का मत है लक िह लनत्यमुक्त, एक, अलद्वतीय और तीनों कािों से अतीत है और देिताओं तथा ऋलषयों आलद को उसी से ज्ञान प्राि होता है। योगदर्शन में संसार को दुःखमय और हेय माना गया है। पुरुष या जीिात्मा क े मोक्ष क े लिये िे योग को ही एकमात्र उपाय मानते हैं। • पतंजलि ने लचत्त की लक्षि, मूढ़, लिलक्षि, लनरुि और एकाग्र ये पााँच प्रकार की िृलत्तयााँ मानी है, लजनका नाम उन्ोंने 'लचत्तभूलम' रखा है।
- 7. • उन्ोंने कहा है लक आरंभ की तीन लचत्तभूलमयों में योग नहीं हो सकता, क े िि अंलतम दो में हो सकता है। • इन दो भूलमयों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये दो प्रकार क े योग हो सकते हैं। लजस अिथथा में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यह योग पााँच प्रकार क े क्लेर्ों का नार् करनेिािा है। • असंप्रज्ञात उस अिथथा को कहते हैं, लजसमें लकसी प्रकार की िृलत्त का उदय नहीं होता अथाशत् ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, संस्कारमात्र बचा रहता है। यही योग की चरम भूलम मानी जाती है और इसकी लसस्ि हो जाने पर मोक्ष प्राि होता है।
- 8. • योगसाधन क े उपाय में यह बतिाया गया है लक पहिे लकसी थथूि लिषय का आधार िेकर, उसक े उपरांत लकसी सूक्ष्म िस्तु को िेकर और अंत में सब लिषयों का पररत्याग करक े चिना चालहए और अपना लचत्त स्थथर करना चालहए। • लचत्त की िृलत्तयों को रोकने क े जो उपाय बतिाए गए हैं िह इस प्रकार हैं:- • अभ्यास और िैराग्य, ईश्वर का प्रलणधान, प्राणायाम और समालध, लिषयों से लिरस्क्त आलद।
- 9. • यह भी कहा गया है लक जो िोग योग का अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकार को लििक्षण र्स्क्तयााँ आ जाती है लजन्ें 'लिभूलत' या 'लसस्ि' कहते हैं। • यम, लनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समालध ये आठों योग क े अंग कहे गए हैं, और योगलसस्ि क े लिये इन आठों अंगों का साधन आिश्यक और अलनिायश कहा गया है। इनमें से प्रत्येक क े अंतगशत कई बातें हैं। कहा गया है जो व्यस्क्त योग क े ये आठो अंग लसि कर िेता है, िह सब प्रकार क े क्लेर्ों से छ ू ट जाता है, अनेक प्रकार की र्स्क्तयााँ प्राि कर िेता है और अंत में क ै िल्य (मुस्क्त) का भागी बनता है।
- 10. यमर्नयमाSSसनप्राणायामप्रत्याहारिारणाध्यानसमाियोSष्टावङ्गार्न १. यम : पांच सामालजक नैलतकता • अर्हांसासत्यास्तेयब्रह्मियािपरग्रहा:यमा • (क) अर्हांसा - अर्हांसाप्रर्तष्ठायाांतत्सर्ििौ वैरत्याग: ।।2/35।। • र्ब्ों से, लिचारों से और कमों से लकसी को हालन नहीं पहुाँचाना। इन पञ्चलिध यमों में र्रीर से प्राण को लियुक्त, पृथक ् करने क े उद्देश्य से लकया गया कायश या चेष्टा लहंसा है और िहीं लहंसा सभी अनथों का मूि कारण है। उसी लहंसा का अभाि अलहंसा है। सभी प्रकार से ही लहंसा का पररत्याग क े योग्य, लहंसा क े त्याज्य होने क े कारण सबसे पहिे उस लहंसा क े अभािरूपी अलहंसा का उल्लेख लकया गया है।
- 11. • (ख) सत्य - सत्यप्रर्तष्ठायाां र्ियाफ़िाश्रययत्वम् ।।2/36 ।। • लिचारों में सत्यता, परम-सत्य में स्थथत रहना। िाणी तथा मन का अथश क े अनुरूप रहना अथाशत् अथश का जैसे स्वरूप है उसी क े अनुसार िाणी से कहना तथा मन से िैसा मनन करना ही सत्य है। • (ग) अस्तेय - अस्तेयप्रर्तष्ठायाां सविरत्नोपस्र्ानम् ।।2/37 ।।चोर-प्रिृलत का न होना। दू सरे क े धन का अपहरण करना ही स्तेय या चोरी हैं। उस स्तेय का अभाि, दू सरे क े धन, सत्त्व का अपहरण न करना ही अस्तेय है।
- 12. • (घ) ब्रह्मियि - ब्रह्मियिप्रर्तष्ठायाां वीयििाि: ।। 2/ 38 ।। • दो अथश हैं:* चेतना को ब्रह्म क े ज्ञान में स्थथर करना* सभी इस्िय-जलनत सुखों में संयम बरतना। मुख्यतः उपथथ इस्िय क े संयम को ब्रह्मचयश कहते हैं। • (च) अपररग्रह - आिश्यकता से अलधक संचय नहीं करना और दू सरों की िस्तुओं की इच्छा नहीं करना। भोग क े साधनों का स्वीकार न करना, ग्रहण न करना ही अपररग्रह है।
- 13. • २. र्नयम: पााँच व्यस्क्तगत नैलतकता • (क) शौि - र्रीर और मन की र्ुस्ि। अथाशत् पलित्रता दो प्रकार की होती है:- बाहरी पलित्रता और आन्तररक र्ौच (अन्तःकरण की पलित्रता/र्ुिता)। लमट्टी, जि इत्यालद से र्रीर इत्यालद क े अङ्ों का धोना, स्वच्छ करना बाह्य स्वच्छता, पलित्रता है। मैत्री इत्यालद अथाशत् मैत्री-करुणा-मुलदता-उपेक्षा क े द्वारा लचत्त में रहने िािे राग-द्वेष, क्रोध-द्रोह-ईष्याश-असूया-मद-मोह-मत्सर-िोभ इत्यालद मिों, किुषों, अर्ुस्ियों का लनराकरण करना ही आन्तररक स्वच्छता, पलित्रता है।
- 14. • (ख) सन्तोष - सन्तुष्ट और प्रसन्न रहना। तुलष्ट ही सन्तोष है। अथाशत् स्वकतशव्य का पािन करते हुये, प्रबन्ध क े ही अनुसार प्राि फि से सन्तुष्ट हो जाना, लकसी प्रकार की तृष्णा का न होना ही सन्तोष है। • (ग) तप - स्वयं से अनुर्ालसत रहना। दू सरे र्ास्त्रों में िणशन लकये गये चािायण इत्यालद तप है। • (घ) स्वाध्याय - आत्मलचंतन करना। प्रणि पूिशक, ओंकार क े साथ मन्त्ों का जप, पाठ करना स्वाध्याय है। • (च) ईश्वर-प्रर्णिान - ईश्वर क े प्रलत पूणश समपशण, पूणश श्रिा। सभी कमों का फि की अलभिाषा, कामना न रखते हुए उस सिशश्रेष्ठ गुरु, ईश्वर में समलपशत करना ईश्वरप्रालणधान है।
- 15. • ३. आसन: योगासनों द्वारा र्ारीररक लनयंत्रण। • स्थथरसुखमासनम् ॥ ४६ ॥ • अथशः-स्थथरसुखं= स्थथर भाि से, लनश्चि रूप से तथा सुखपूिशक बैठने को, आसनं = आसन कहते हैं। • अथिा लजसक े द्वारा स्थथरता तथा सुख की प्रास्ि हो, िह आसन है। इसक े द्वारा स्थथरभाि से तथा सुखपूिशक बैठा जाता है इसलिये इसे आसन कहते हैं। • यथा- पद्मासन, दण्डासन, स्वस्स्तकासन इत्यालद।
- 16. 4.प्राणायाम • तस्मिन् सर्त श्वासप्रश्वासयोगिर्तर्वच्छेद: प्राणायाम: ।। पातांजियोगदशिन 2/49 ।। • उस ( आसन) क े लसि होने पर श्वास और प्रश्वास की गलत को रोकना प्राणायाम है । • योग की यथेष्ट भूलमका क े लिए नाड़ी साधन और उनक े जागरण क े लिए लकया जाने िािा श्वास और प्रश्वास का लनयमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचिता और लिक्षुब्धता पर लिजय प्राि करने क े लिए बहुत सहायक है।
- 17. • प्रत्याहार • इस्ियों को अंतमुशखी करना महलषश पतंजलि क े अनुसार जो इस्ियां लचत्त को चंचि कर रही हैं, उन इस्ियों का लिषयों से हट कर एकाग्र हुए लचत्त क े स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इस्ियां िर् में रहती हैं और उन पर पूणश लिजय प्राि हो जाती है। अतः लचत्त क े लनरुि हो जाने पर इस्ियां भी उसी प्रकार लनरुि हो जाती हैं, लजस प्रकार रानी मधुमक्खी क े एक थथान पर रुक जाने पर अन्य मधुमस्क्खयां भी उसी थथान पर रुक जाती हैं।
- 18. • िारणा • मन को एकाग्रलचत्त करक े ध्येय लिषय पर िगाना पड़ता है। लकसी एक लिषय का ध्यान में बनाए रखना। • ध्यान • लकसी एक थथान पर या िस्तु पर लनरन्तर मन स्थथर होना ही ध्यान है। जब ध्येय िस्तु का लचन्तन करते हुए लचत्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूणश ध्यान की स्थथलत में लकसी अन्य िस्तु का ज्ञान अथिा उसकी स्मृलत लचत्त में प्रलिष्ट नहीं होती।
- 19. • समार्ि • यह लचत्त की अिथथा है लजसमें लचत्त ध्येय िस्तु क े लचंतन में पूरी तरह िीन हो जाता है। योग दर्शन समालध क े द्वारा ही मोक्ष प्रास्ि को संभि मानता है। समालध की भी दो श्रेलणयााँ हैं : सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात समालध लितक श , लिचार, आनन्द और अस्स्मतानुगत होती है। असम्प्रज्ञात में सास्िक, राजस और तामस सभी िृलत्तयों का लनरोध हो जाता है।
- 20. र्ित्त र्वक्षेप 'योगान्तराय' • लचत्त लिक्षेपों को ही ‘योगान्तराय’ कहते है जो लचत्त को लिलक्षि करक े उसकी एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं उन्ें योगान्तराय अथिा योग क े लिध्न कहा जाता। 'योगस्य अन्तः मध्ये आयास्मन्त ते अन्तरायाः'। ये योग क े मध्य में आते हैं इसलिये इन्ें योगान्तराय कहा जाता है। लिघ्ों से व्यलथत होकर योग साधक साधना को बीच में ही छोड़कर चि देते हैं।
- 21. • व्यालधस्त्यानसंर्यप्रमादािस्यालिरलतभ्रास्न्तदर्शनािब्धभूलमकिानिस्थथतिालन लचत्तलिक्षेपास्तेऽन्तरायाः (योगसूत्र - 1/30) • योगसूत्र क े अनुसार लचत्त लिक्षेपों या अन्तरायों की संख्या नौ हैं- व्यालध, स्त्यान, संर्य, प्रमाद, आिस्य, अलिरलत, भ्रास्न्तदर्शन, अिब्धभूलमकि और अनिस्थथति। उक्त नौ अन्तराय ही लचत्त को लिलक्षि करते हैं। • अतः ये योगलिरोधी हैं इन्ें योग क े मि भी कहा जाता हैं। लचत्तिृलत्तयों क े साथ इनका अन्वयव्यलतरेक है। अथाशत् इन लिक्षेपों क े होने पर प्रमाणालद िृलत्तयााँ होती हैं। जब ये नहीं होते तो िृलत्तयों भी नहीं होती। िृलत्तयों क े अभाि में लचत्त स्थथर हो जाता है। इस प्रकार लचत्तलिक्षेप क े प्रलत ये उक्त नौ अन्तराय ही कारण हैं।
- 22. • 1. व्यार्ि- 'िातुरसकरणवैषम्यां व्यार्ि” • धातुिैषम्य, रसिैषम्य तथा करणिैषम्य को व्यालध कहते हैं। िात, लपत्त और कफ ये तीन धातुएं हैं। इनमें से यलद एक भी क ु लपत होकर कम या अलधक हो जाये तो िह धातुिैषम्य कहिाता है। जब तक देह में िात, लपत्त और कफ समान मात्रा में हैं तो तब इन्ें धातु कहा जाता हैं। जब इनमें लिषमता आ जाती है तब इन्ें दोष कहा जाता है।
- 23. • धातुओं की सम अिथथा में र्रीर स्वथथ रहता है। धातुओं की लिषमता में र्रीर रुग्ण हो जाता है। आहार का अच्छी तरह से पररपाक न होना रसिैषम्य कहिाता है। यही र्रीर में व्यालध बनाता है। ज्ञानेस्ियों तथा कमेस्ियों की र्स्क्त का मन्द हो जाना करणिैषम्य है। योगसाधना क े लिए सर्क्त और दृढ़ इस्ियों की आिश्यकता होती है। धातु, रस तथा करण इन तीनों की लिषमता को ही व्यालध कहते हैं। रोगी र्रीर से समालध का अभ्यास सम्भि नहीं। अतः व्यालध समालध क े लिए अन्तराय है। कफ, श्वास आलद दैलहक रोगों को व्यालध कहते हैं तथा मानलसक रोग को आलध जैसे स्मरण र्स्क्त का अभाि, उनन्माद, अरुलच, घृणा, काम, क्रोध आलद। आलध र्ब् क े 'लि! उपसगश क े योग से व्यालध र्ब् बनता है 'लिर्ेषेण आधीयते अनुभूयते मनसा इलत व्यालधः चूाँलक र्ारीररक रोग मन को आलध की तुिना में अलधक कष्टकारक अनुभूत होता है, इसलिए र्ारीररक रोग का व्यालध नाम साथशक लसि होता है।
- 24. • 2. स्त्यान- 'स्त्यानां अकमिण्यता र्ित्तस्य' अर्ाित् र्ित्त की अकमिण्यता को स्त्यान कहते हैं। • समालध का अभ्यास करने की इच्छा तो लचत्त में होती है लकन्तु िैसा सामर्थ्श उसमें नहीं होता। क े िि इच्छा से योग लसि नहीं होता, अलपतु उसमें योगाभ्यास की र्स्क्त होनी चालहए। पुत्रों की आसस्क्त, लिषयभोग की िािसाएं तथा जीलिकाोपाजशन क े व्यापार में लचत्त को उिझाये रखते हैं लजससे लक लचत्त अकमशण्यता अनुभि करता है। अकमशण्यता समालध में अन्तराय है। जब तक सत्यान की अिथथा रहेगी तब तक साधक क े लिये समालध का मागश अिरूि रहेगा।
- 25. • 3. सांशय- “उियकोर्िस्पृग् र्वज्ञानां सांशयः' अर्ाित् यह िी हो सकता है और वह िी हो सकता है। • इस प्रकार क े ज्ञान को संर्य कहते हैं। योग साधना क े लिषय में जब साधक को कभी कभी संर्य होता है लक मैं योग का अभ्यास कर सक ूं गा या नहीं क्या मुझे सफिता लमिेगी क्या मुझे समालध (क ै िल्य) प्राि हो सकता है मेरा पररश्रम व्यथश तो नही चिा जायेगा, तब यह संर्यात्मक ज्ञान योग का लिध्न बन जाता है। संर्य की अिथथा में साधक का लचत्त असंतुलित रहता है और िह साधना नहीं कर सकता है।
- 26. • 4. प्रमाद- 'समार्िसािनानामिावनम्' समार्ि क े सािनोां में उत्साह पूविक प्रवृर्त्त न होना प्रमाद कहिाता है। • समालध का अभ्यास प्रारम्भ कर देने पर उसमें िैसा ही उत्साह और दृढ़ता लनरन्तर बनी रहनी चालहए जैसा उत्साह प्रारम्भ में था। प्रायः युिािथथा का मद, धन और प्रभुि का दपश तथा र्ारीररक सामर्थ्श का मद साधक क े उत्साह को लर्लथि कर देता है। अतः प्रमाद समालध में अन्तराय है।
- 27. • 5. आिस्य- 'आिस्यां कायस्य र्ित्तस्य ि गुरुत्वादप्रवृर्त्तः काम क े आर्िक्य से शरीर तर्ा तमोगुण क े आर्िक्य से र्ित्त िारीपन का अनुिव करता है। • र्रीर और लचत्त क े भारी होने से समालध क े साथनों में प्रिृलत्त नहीं होती, इसी का नाम आिस्य है। प्रमाद और आिस्य में बहुत अन्तर है। प्रमाद प्रायः अलििेक से उत्पन्न होता है। आिस्य में अलििेक तो नहीं होता लकन्तु गररष्ठ भोजन क े सेिन से र्रीर और लचत्त भारी हो जाता है। यह भी योग साधना मागश में अन्तराय कहिाता है।
- 28. • 6. अर्वरर्त- “र्ित्तस्य र्वषयसम्प्रयोगात्मा गिि: अर्वरर्तः कोमिकान्त िचन, उनक े अंगों का मोहक स्पर्श, तथा स्वालदष्ट भोज्य, पेय आलद व्यंजनों का रस कभी कभी तत्त्वज्ञान को भी आिृत्त करक े साधक को संसार में आसक्त बना देता है। • लिषयों क े प्रलत यह आसस्क्त ही अलिरलत है। यह अलिरलत योग का महान् लिध्न कहा गया है। जब तक अलिरलत रहेगी तब तक लचत्त िृलत्तयों का लनरोध नहीं हो सकता है। र्ब्ालद लिषयों क े भोग से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा िैराग्य की र्त्रु है। समालध क े लिये िैराग्य प्रमुख साधन है। अतः िैराग्य का अभाि योग का अन्तराय है।
- 29. • 7. भ्रास्मन्तदशिन- “िास्मन्तदशिनां र्वपयियज्ञानम्' अथाशत् लमर्थ्ाज्ञान को भ्रास्न्तदर्शन कहते हैं। अन्य िस्तु में अन्य िस्तु का ज्ञान ही लमर्थ्ा ज्ञान है। • जब साधक योग क े साधनों को असाधन और असाधनों को साधन समझने िगता है तो यह भास्न्तदर्शन योग का लिध्न बन जाता है। भ्रास्न्तदर्शन में व्यस्क्त को साधन क े फिों में झूठा ज्ञान हो जाता है।
- 30. • 8. अिब्धिूर्मकत्व- 'अिब्धिूर्मकत्व समार्ििूमेरिाि: • अथाशत् समालध की लकसी भी भूलम की प्रास्ि न होना भी योग में लिघ् है। समालध की चार भूलमयााँ हैं सलितक श , लनलिशतक, सलिचार तथा लनलिशचार। जब प्रथम भूलम की प्रास्ि हो जाती है तो योगी का उत्साह बढ़ जाता है। • िह सोचता है लक जब प्रथम भूलम प्राि हो गयी है तो अन्य भूलमया भी अिश्य ही प्राि होंगी। परन्तु लकसी कारण से उनकी प्रास्ि न होना अिब्धभूलमकि कहा गया है। यह भी योग में अन्तराय है।
- 31. • 9. अनवस्मस्र्तत्व- “िब्धायाां िूमाूँ र्ित्तस्याप्रर्तष्ठा अनवस्मस्र्तत्वम्’ • यलद लकसी प्रकार समालध की भूलमयों में से लकसी एक की प्रास्ि हो जाये लकन्तु उसमें लनरन्तर लचत्त की स्थथलत न हो तो यह अनिस्थथति कहिाता है। • इस प्रकार ये नौ लचत्तलिक्षेप योग क े अन्तराय कहिाते हैं। इन्ीं को लचत्तमि तथा योग प्रलतपक्ष भी कहा गया है।
- 32. र्ित्त र्वक्षेप सहिुवः • इन लचत्तलिक्षेपों क े पााँच साथी भी हैं। जो इन अन्तरायों क े होने पर स्वतः हो जाते हैं दुःखदौमिनस्यअांगमेजयत्वश्वासप्रश्वास र्वक्षेपसहिुवः (योगसूत्र- 1/31) • 1. दुःख- दुःख क े बारे में व्यास जी कहते हैं “येनालभहताः प्रालणनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद् दु:खम' (योगसूत्र व्यासभाष्य 1/31)
- 33. • लजसक े साथ सम्बन्ध होने से पीलड़त हुए प्राणी उस प्रलतक ू ि िेदनीय हेय दुःख की लनिृलत्त क े लिए प्रयत्न करते हैं, िह दुःख कहा जाता है। • दु:ख तीन प्रकार क े हैं आध्यास्त्मक, आलदभौलतक तथा आलधदैलिक। • आध्यास्त्मक दुख भी दो प्रकार क े होते हैं- र्ारीररक और मानलसक। लकसी भी प्रकार का र्ारीररक रोग जैसे कब्ज, अपच, पीलिया, रक्तचाप, अथथमा इत्यालद तथा मानलसक रोग लचन्ता, तनाि अिसाद आलद ये आध्यास्त्मक दु:ख कहिाते है लजनक े कारण भी योग साधना में बाधा उत्पन्न होती है।
- 34. • आलदभौलतक र्ब् की रचना का लिचार लकया जाए तो ज्ञात होता है लक यह र्ब् भूत र्ब् से बना है। भूत र्ब् का अथश है प्राणी अथाशत प्रालणयों क े द्वारा लदये गए दुःखों को आलदभौलतक कहा जाता है। • प्राणी, योलनज, स्वेदज, अण्डज तथा उस्िज भेद से चार प्रकार क े होते हैं। • दुःखों क े तृतीय प्रकार का नाम आलददैलिक है लजसका अथश है दैलिक र्स्क्तयों क े द्वारा लदये गए दुःख। • दैलिक र्स्क्तयों क े रूप में अलि, जि और िायु की गणना की जाती है। ये तीनों प्रत्येक क े लिए अलत आिश्यक हैं परन्तु आिश्यकता से अलधक या कम होने पर ये दुःखों क े उत्पादक होते हैं।
- 35. • 2. दौमिनस्य- • अलभिलक्षत पदाथश लिषयक इच्छा की पूलतश न होने से लचत्त में जो क्षोभ उत्पन होता है। उसे दौमशनस्य कहा जाता है। • जब प्रयास करने पर भी इच्छा की पूलतश नहीं होती तो लचत्त व्याक ु ि होता है। यह दौमशनस्य भी दुःख का साथी है। • इच्छाव्याघातात् चेतसः क्षोभः दौमशनस्यम्। (योगसूत्र व्यासभाष्य 1/31)
- 36. • िास्ति में इच्छापूलतश न होने पर व्यस्क्त की स्थथलत अलत भयंकर हो जाती है। ितशमान प्रलतस्पधाश क े युग में व्यस्क्त में उच्चतम महिाकाक्षायें रहती है तथा कमश का अभाि है ऐसी लिषम पररस्थथलत में दौमशन्य का होना स्वाभालिक है ऐसी स्थथलत में साधक पहिे तो साधना करता ही नहीं है अगर करता भी है तो दौमशनस्य होने पर उसे छोड़ देता है यह दौमशनस्य योग में सबसे बड़ा लिध्न है।
- 37. • 3. अांगमेजयत्व- • जो र्रीर क े हाथ, पैर , लसर आलद अंगों की कस्ित अिथथा है, िह अंगमेजयत्य कहिाती है • यत् अांगार्न एजयर्त कम्पयर्त तद् अांगमेजयत्यम् • व्यालध आलद अन्तराय र्रीर को दुबशि बना देती हैं लजससे अंगों में किन होने िगता है। यह अंगमेजयि आसन, प्राणायाम आलद में व्यिधान उपस्थथत करता है। • अतः लिक्षेप का साथी होने से समालध का प्रलतपक्षी है। िातरोग होने क े कारण देखा गया है लक र्रीर क े अंगों में किन हो जाता है व्यास्क्त को िकिा हो जाता है यह भी योग में लिघ् है।
- 38. • 4. श्वास- • लजस बाह्य िायु का नालसकाग्र क े द्वारा आचमन करते है, िह श्वास कहिाता है अथाशत् भीतर की ओर जाने िािा प्राणिायु श्वास है। यह प्राणलक्रया यलद लनरन्तर चिती रहे, क ु छ समय क े लिए भी न रुक े तो लचत्त समालहत नही रह सकता। यह श्वास रेचक प्राणायाम का लिरोधी होता है। अतः यह समालध प्रास्ि में अन्तराय है।. • 5. प्रश्वास- • जो प्राण भीतर की िायु को बाहर लनकािता है, िह प्रश्वास कहिाता है। यह श्वास लक्रया भी लनरन्तर चिती रहती है। यह भी समालध क े अंगभूत पूरक प्राणायाम का लिरोधी होने से समालध का लिरोधी है। अतः लिक्षेप का साथी होने से योगान्तराय कहा जाता है।
- 39. • तत्प्रर्तषेिार्िमेकतत्त्वाभ्यासः (योगसूत्र-1/32) अथाशत् उक्त योगान्तरायों क े लनराकरण क े लिये साधक को ईश्वररूप एक ति क े लचन्तन में पुनः पुनः लचत्त को प्रलिष्ठ करने का अभ्यास करना चालहए। एकतत्त्वाभ्यास का अथश है 'ईश्वरप्रलणधान'। ईश्वरप्रलणधान का अभ्यास करने से कोई भी लिघ् योगमागश में उपस्थथत नहीं होता।